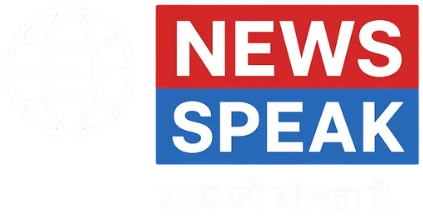भारत की शिक्षा प्रणाली एक गंभीर और स्थायी चुनौती से जूझ रही है: देश भर में 1.17 लाख से अधिक स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम यूडीआईएसई+ (Unified District Information System for Education Plus) रिपोर्ट के अनुसार, इन single-teacher schools में लगभग 34 लाख छात्र नामांकित हैं, जो शिक्षा की गुणवत्ता, समान अवसर और बच्चों के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
मुख्य तथ्य / त्वरित जानकारी
- कुल एकल-शिक्षक स्कूल: भारत में कुल 1,17,548 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक द्वारा चलाए जा रहे हैं (यूडीआईएसई+ 2023-24)।
- प्रभावित छात्र: इन स्कूलों में लगभग 34 लाख बच्चे पढ़ते हैं, जिनका सीखना-सिखाना एक ही शिक्षक पर निर्भर है।
- राज्यों की स्थिति: आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक (14,120) एकल-शिक्षक स्कूल हैं, इसके बाद तेलंगाना (11,350) और मध्य प्रदेश (10,560) का स्थान है।
- छात्रों की संख्या में: इन स्कूलों में सबसे ज्यादा छात्र उत्तर प्रदेश (लगभग 5.1 लाख) और बिहार (लगभग 4.3 लाख) में नामांकित हैं।
- नीति का उल्लंघन: यह स्थिति शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के कई मानदंडों का उल्लंघन करती है, जो छात्र-शिक्षक अनुपात और न्यूनतम शिक्षक संख्या निर्धारित करता है।
क्या है पूरा मामला?
भारत सरकार जहाँ एक ओर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के माध्यम से 21वीं सदी के लिए वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने का लक्ष्य रखती है, वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां करती है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी यूडीआईएसई+ 2023-24 की रिपोर्ट (स्रोत: शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट) ने इस विरोधाभास को उजागर किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि देश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों में स्थित हजारों स्कूल आज भी औपनिवेशिक युग की ‘एक शिक्षक’ वाली व्यवस्था में अटके हुए हैं।
ये स्कूल, जिन्हें अक्सर ‘एकल-शिक्षक विद्यालय’ कहा जाता है, वे हैं जहाँ एक ही शिक्षक को एक साथ कई कक्षाओं (आमतौर पर कक्षा 1 से 5 तक) के छात्रों को पढ़ाना होता है। इसके अलावा, उसे मिड-डे मील का प्रबंधन, प्रशासनिक कार्य, दाखिले और अन्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसी गैर-शैक्षणिक जिम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं। यह स्थिति न केवल शिक्षक पर भारी बोझ डालती है, बल्कि छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को भी गंभीर रूप से बाधित करती है।
नवीनतम आँकड़े: एक गहरी खाई
आँकड़े इस समस्या की भयावहता को स्पष्ट करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में स्थिति में मामूली सुधार के बावजूद, यह चुनौती बनी हुई है।
तालिका: शीर्ष 5 राज्यों में एकल-शिक्षक स्कूलों की स्थिति (2023-24)
| राज्य | एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या | प्रभावित छात्रों की अनुमानित संख्या |
| आंध्र प्रदेश | 14,120 | 2.9 लाख |
| तेलंगाना | 11,350 | 2.5 लाख |
| मध्य प्रदेश | 10,560 | 3.8 लाख |
| राजस्थान | 9,880 | 3.1 लाख |
| उत्तर प्रदेश | 8,550 | 5.1 लाख |
स्रोत: यूडीआईएसई+ 2023-24 रिपोर्ट के विश्लेषण पर आधारित।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जहाँ आंध्र प्रदेश में स्कूलों की संख्या सबसे अधिक है, वहीं उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी आबादी वाले राज्य में इन स्कूलों में नामांकित छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। यह दर्शाता है कि समस्या का प्रभाव व्यापक है। पिछले वर्ष (2022-23) के आंकड़ों से तुलना करने पर, एकल-शिक्षक स्कूलों की संख्या में लगभग 2% की मामूली कमी देखी गई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह गति बेहद धीमी है।
आधिकारिक प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों का विश्लेषण
सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार किया है। जुलाई 2025 में संसद में एक प्रश्न के उत्तर में, शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती और युक्तिकरण राज्यों का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार समग्र शिक्षा जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “सरकार शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज पर विचार कर रही है।”
हालांकि, शिक्षा विशेषज्ञ इस प्रतिक्रिया को अपर्याप्त मानते हैं। प्रथम फाउंडेशन के एक वरिष्ठ शोधकर्ता डॉ. अविनाश कुमार कहते हैं:
“यह केवल शिक्षकों की कमी का मामला नहीं है, बल्कि यह व्यवस्थागत विफलता है। एक शिक्षक एक साथ पाँच कक्षाओं को कैसे न्याय दे सकता है? यह आरटीई अधिनियम की आत्मा का उल्लंघन है, जो आयु-उपयुक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देता है। हमें स्कूल-कॉम्प्लेक्स और क्लस्टरिंग जैसे मॉडलों को प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है, जैसा कि एनईपी 2020 में सुझाया गया है।”
विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह स्थिति सीधे तौर पर सीखने के परिणामों (Learning Outcomes) को प्रभावित करती है। असर (ASER) की रिपोर्टें लगातार दिखाती रही हैं कि ग्रामीण भारत में कई छात्र अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप पढ़ने और गणितीय कौशल में पीछे हैं। एकल-शिक्षक स्कूल इस समस्या को और बढ़ाते हैं।
जमीनी हकीकत: एक शिक्षक का संघर्ष
राजस्थान के एक दूरदराज के गाँव के एकमात्र शिक्षक रामभरोस मीणा (बदला हुआ नाम) अपनी दैनिक चुनौतियों को साझा करते हैं। “सुबह स्कूल खोलने से लेकर, प्रार्थना, हाजिरी, पाँच अलग-अलग कक्षाओं के लिए पाठ योजना बनाने, मिड-डे मील की निगरानी करने और फिर शाम को रजिस्टर मेंटेन करने तक, सब कुछ मुझे अकेले ही करना पड़ता है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो स्कूल बंद रहता है।” (स्रोत: एक स्थानीय समाचार रिपोर्ट से उद्धृत)।
ऐसी स्थिति में, बच्चों को व्यक्तिगत ध्यान नहीं मिल पाता है, खासकर उन बच्चों को जिन्हें सीखने में अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। बहु-स्तरीय शिक्षण (Multi-level teaching) एक विशेष कौशल है जिसके लिए गहन प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश शिक्षकों के पास नहीं होता है। इसका परिणाम यह होता है कि बच्चे केवल अक्षर और अंक पहचानना सीखते हैं, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण सोच और समस्या-समाधान की क्षमता विकसित नहीं हो पाती है।
आगे की राह और निष्कर्ष
इस गंभीर समस्या का समाधान बहुआयामी दृष्टिकोण की मांग करता है:
- तत्काल भर्ती: राज्यों को मिशन मोड में शिक्षकों के खाली पदों को भरना होगा।
- स्कूलों का युक्तिकरण: कम नामांकन वाले आस-पास के स्कूलों को मिलाकर ‘स्कूल कॉम्प्लेक्स’ बनाना और संसाधनों को साझा करना एक प्रभावी समाधान हो सकता है।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग: दूरस्थ शिक्षा और डिजिटल संसाधनों का उपयोग करके शिक्षकों और छात्रों दोनों की मदद की जा सकती है।
- शिक्षकों के लिए प्रोत्साहन: ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में सेवा देने वाले शिक्षकों के लिए बेहतर वेतन, आवास और अन्य प्रोत्साहन प्रदान किए जाने चाहिए।
निष्कर्षतः, 1.17 लाख एकल-शिक्षक स्कूलों का अस्तित्व भारत की शैक्षिक आकांक्षाओं पर एक धब्बा है। यह न केवल लाखों बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित करता है, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा देता है। यदि भारत को वास्तव में एक ज्ञान आधारित समाज बनना है, तो उसे अपनी नींव, यानी प्राथमिक शिक्षा को मजबूत करना होगा, और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी स्कूल केवल ‘एक शिक्षक’ के भरोसे न रहे।